भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13: जब कानून संविधान से टकराता है | विश्लेषणात्मक न्यूज़ ब्लॉग
📢 We News 24 / वी न्यूज 24
📲 वी न्यूज 24 को फॉलो करें और हर खबर से रहें अपडेट!
👉 ताज़ा खबरें, ग्राउंड रिपोर्टिंग, और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़ें हमारे साथ।
लेखक: वरिष्ट पत्रकार दीपक कुमार / संपादकीय डेस्क
क्या कोई कानून संविधान से बड़ा हो सकता है? अगर कोई नियम या अधिनियम हमारे मौलिक अधिकारों पर चोट करता है, तो क्या वह वैध माना जाएगा? यही सवालों का जवाब देता है — भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13। यह एक ऐसा प्रावधान है, जो न केवल कानून की वैधता को तय करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून, चाहे वह नया हो या पुराना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे।
अनुच्छेद 13: क्या कहता है संविधान?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 "कानूनों की संविधान के साथ संगति" से संबंधित है। यह संविधान के भाग III में आता है, जो मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) से संबंधित है। इसकी भाषा स्पष्ट और सख्त है — कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, वह अमान्य माना जाएगा।
अनुच्छेद 13 के मुख्य प्रावधान:
13(1) — मौजूदा कानूनों की अमान्यता:
स्वतंत्रता के समय लागू सभी पुराने कानून, अगर वे मौलिक अधिकारों से असंगत पाए जाएं, तो वे उस हद तक अमान्य होंगे।
13(2) — भविष्य के कानूनों पर प्रतिबंध:
राज्य को यह अधिकार नहीं कि वह ऐसा कोई कानून बनाए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। ऐसा कोई कानून स्वतः अमान्य होगा।
13(3) — 'कानून' की परिभाषा:
इसमें अधिनियम, अध्यादेश, नियम, विनियम, अधिसूचना और यहाँ तक कि परंपरागत रीति-रिवाज भी शामिल हैं। यानी, किसी भी रूप में नागरिकों की स्वतंत्रता को चोट पहुँचाने वाला प्रावधान संविधान विरोधी हो सकता है।
13(4) — संविधान संशोधन की छूट:
1971 के 24वें संविधान संशोधन के बाद यह स्पष्ट किया गया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के दायरे में नहीं आएगा। यानी संसद संविधान संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह मौलिक ढांचे (Basic Structure) को क्षति न पहुँचाए।
ये भी पढ़े-वक्फ कानून 2013: क्या संविधान की आड़ में वोटबैंक की राजनीति?" | संपादकीय विशेष रिपोर्ट
ऐतिहासिक संदर्भ और प्रमुख मामले:
के. शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951):
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 में नहीं आता।
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967):
कोर्ट ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि संसद को संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 13(2) का उल्लंघन होगा।
24वां संशोधन (1971):
सरकार ने गोलकनाथ फैसले को पलटने के लिए संशोधन किया और स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत 'कानून' नहीं माना जाएगा।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):
यह मामला 'मौलिक ढांचे' की अवधारणा का जन्मदाता बना। कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन हो सकता है लेकिन मौलिक ढांचे को क्षति नहीं पहुँचाई जा सकती।
ये भी पढ़े-"क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम जनसंख्या की नहीं, समस्याओं की जनगणना करें?"
उदाहरण के रूप में समझें:
मान लीजिए कोई कानून बनता है जो बोलने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है। यदि वह प्रतिबंध न्यायसंगत नहीं है, तो अनुच्छेद 13 के तहत वह कानून अमान्य घोषित किया जा सकता है।
इसी तरह, अगर कोई राज्य अधिनियम जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, तो वह अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करेगा और अनुच्छेद 13 उसे अमान्य कर देगा।
अनुच्छेद 13 क्यों है जरूरी?
ये भी पढ़े-जब न्याय तक पहुंच भी वंश से तय हो — क्या यही है लोकतंत्र का सपना?”
निष्कर्ष:
अनुच्छेद 13 भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यह संविधान को महज एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवंत व संवेदनशील संरचना बनाता है, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार सर्वोच्च माने जाते हैं।
यह अनुच्छेद हमें यह सिखाता है कि कानून का उद्देश्य केवल शासन चलाना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। अगर कोई भी कानून उस न्याय से भटकता है, तो संविधान उसे नकार देता है।
संविधान सर्वोच्च है, और कोई भी कानून उसके विपरीत नहीं हो सकता।
यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है।
अनुच्छेद 13 नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाला एक मूलभूत सुरक्षा कवच है।
इस प्रकार, भारतीय संवैधानिक ढाँचे में संविधान सबसे ऊपर है, और कोई भी कानून उसकी मूल भावना के विरुद्ध नहीं जा सकता।
क्योंकि संविधान का हर अक्षर कहता है: नागरिक सर्वोपरि हैं, न कि सत्ता।
(यह लेख We News 24 Hindi द्वारा संविधानिक जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है।)

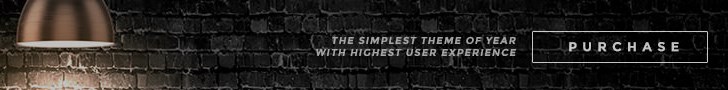






कोई टिप्पणी नहीं
कोमेंट करनेके लिए धन्यवाद